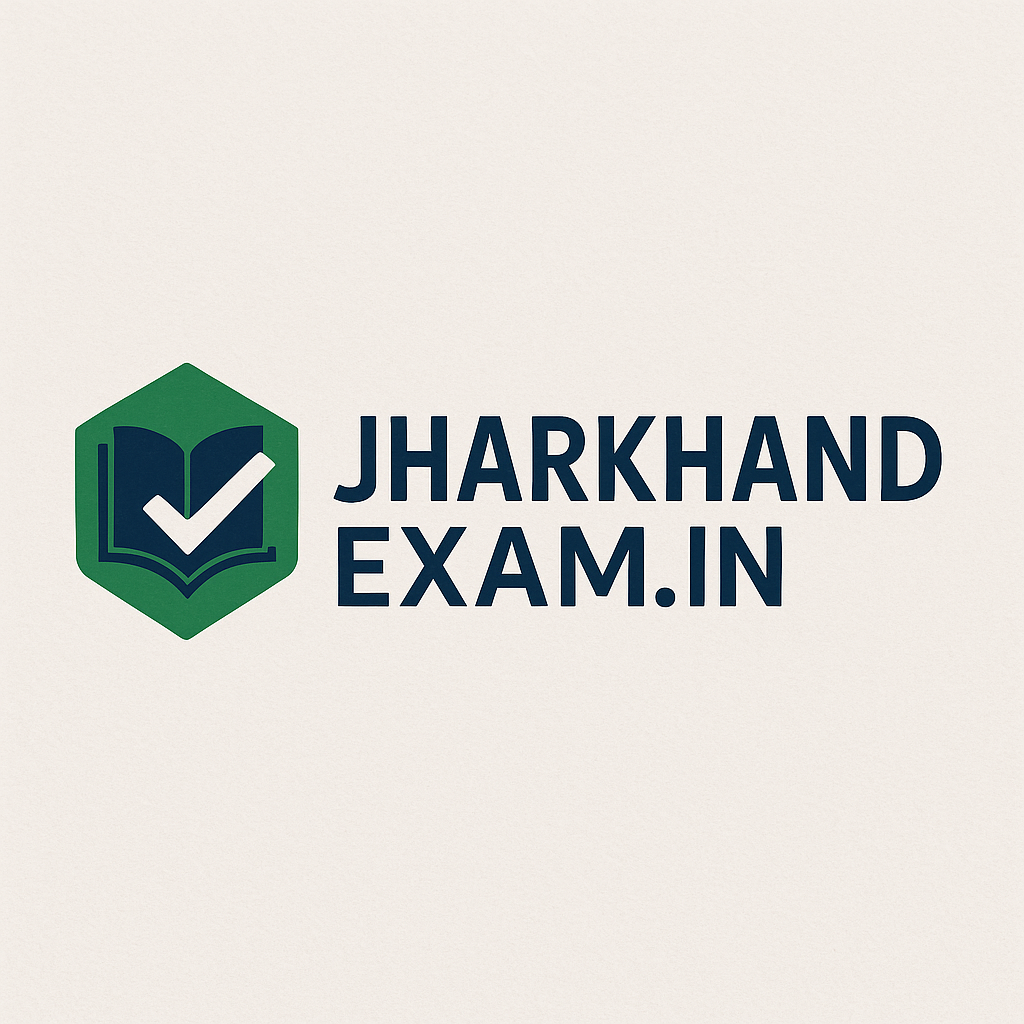झारखंड में मुगलोत्तर काल (1707-1765)
- औरंगज़ेब की मृत्यु (1707) के बाद मुग़ल साम्राज्य कमजोर हुआ, जिससे झारखंड में भी अराजकता बढ़ी।
- रामगढ़, पलामू और छोटानागपुर के इलाकों में स्थानीय राजा और जमींदारों ने अपनी सत्ता मजबूत करने की कोशिश की।
- रामगढ़ राजा को बंगाल के सूबेदार से ‘मनसब’ प्राप्त था, लेकिन धीरे-धीरे रामगढ़ स्वतंत्र व्यवहार करने लगा।
- छोटानागपुर में भी नागवंशी राजा मुग़ल प्रतिनिधियों से स्वतंत्रता की भावना रखने लगे थे।
- पलामू में चेरो शासक मुग़लों के अधीन थे लेकिन समय के साथ वहां भी सत्ता संघर्ष उभरने लगे।
- सिंहभूम में स्थानीय शासक लगभग स्वतंत्र थे और मुग़ल नियंत्रण बहुत कमज़ोर था।
- बंगाल के नवाबों (जैसे मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां) ने कोशिश की कि झारखंड क्षेत्र पर कर वसूली और राजनीतिक नियंत्रण बना रहे, लेकिन वे पूरी तरह सफल नहीं हो पाए।
- बार-बार विद्रोह और स्थानीय संघर्ष की स्थिति बनी रही, जिससे क्षेत्रीय सत्ता बिखरी रही।
- 18वीं सदी के मध्य तक झारखंड का बड़ा हिस्सा नाम मात्र का मुग़ल या नवाबी अधीन रहा; असली नियंत्रण स्थानीय राजाओं के हाथों में था।
आधुनिक काल (1765–1942)
दीवानी और झारखंड की स्थिति
- 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कम्पनी को 26 लाख वार्षिक कर पर प्रदान की।
- झारखंड (तत्कालीन छोटानागपुर क्षेत्र) बिहार में शामिल था, लेकिन यह क्षेत्र बिहार-बंगाल से भिन्न था।
- मुगलों और मराठों ने यहां समय-समय पर हमले किए परंतु स्थायी शासन स्थापित नहीं कर सके।
- स्थानीय राजा स्वतंत्र रूप से शासन करते रहे; अंग्रेजों का हस्तक्षेप धीरे-धीरे बढ़ा।
अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश
सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश (1760)
- मिदनापुर पर कब्जा जमाने के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम में रुचि ली।
- सिंहभूम के तीन प्रमुख राज्य थे:
- ढालभूम (ढाल राजाओं का क्षेत्र)
- पौरहाट (सिंह राजाओं का क्षेत्र)
- कोल्हान (हो जनजाति का क्षेत्र)
विद्रोहियों की शरणस्थली: सिंहभूम, टमर, पटकुम और बाराभूम
- ब्रिटिश आगमन से पहले, पूर्वी सिंहभूम, छोटानागपुर प्रॉपर, टमर, पटकुम और बाराभूम विद्रोहियों की शरणस्थली बन चुके थे।
- कोल्हान के कोल योद्धा छोटानागपुर प्रॉपर, गंगपुर, बोनई, क्योंझर और बामनघाटी पर हमले करते थे।
- लगातार हमलों से परेशान होकर पोरहाट के राजा ने ब्रिटिशों से सुरक्षा मांगी।
हज़ारीबाग क्षेत्र में विखंडित शासन
- मध्यकालीन काल में हज़ारीबाग में छोटे-छोटे राज्य थे:
- रामगढ़
- कुंडा
- केंदी
- छै
- खरकडीहा
- 1677–1724 के दौरान दलेल सिंह ने रामगढ़ पर शासन किया।
- 1718 में दलेल सिंह ने छै के राजा मघर खान को हराकर उसकी हत्या की और कब्जा किया:
- बीघा (राजधानी)
- जगोदीह परगना
- आठ अन्य तालुके
- 1717–1724 तक छै दलेल सिंह के अधीन रहा।
- 1719 में दलेल सिंह ने नागवंशी राजा की मदद कर पलामू के चेरो राजा रंजीत सिंह से तोरी परगना छीना।
- बाद में मघर खान के पुत्र रनमस्त खान ने क्षेत्रों को पुनः हासिल कर लिया।
- उसी वर्ष दलेल सिंह की मृत्यु हो गई और विष्णु सिंह उत्तराधिकारी बना।
विष्णु सिंह की साजिशें और अवज्ञा
- विष्णु सिंह ने छल से छै को फिर से अधीन किया।
- महिपत खान ने सहायता मांगी:
- इतखोरी के राजा शत्रुघ्न सिंह से
- टेकारी के राजा सुंदर सिंह से
- विष्णु सिंह को पकड़ा गया लेकिन ₹10,000 की रिश्वत देकर वह छूट गया।
- टेकारी राजा ने बीघा और आठ तालुके जब्त कर लिए और पाँच साल तक रखे।
- विष्णु सिंह ने बंगाल के नवाब की अवज्ञा की और कर देना बंद कर दिया।
बंगाल की प्रतिक्रिया: हिदायत अली खान का अभियान
- 1740 में नवाब अलीवर्दी खान ने हिदायत अली खान को भेजा।
- विष्णु सिंह की हार हुई और उसे देना पड़ा:
- ₹80,000 की बकाया राशि
- कुछ नकद और कुछ भूमि के रूप में
- रामगढ़ का वार्षिक कर ₹12,000 तय हुआ।
छै की लड़ाई: महिपत खान की वंशावली की वापसी
- 1747 तक विष्णु सिंह का छै पर नियंत्रण रहा।
- महिपत खान की मृत्यु के बाद:
- उत्तराधिकारी बना लाल खान
- रतन सिंह (रामपुर के ज़मींदार) और लाल खान ने कामगार खान से मदद ली
- कामगार खान ने रामगढ़ पर हमला कर विष्णु सिंह को हराया।
- रतन सिंह और लाल खान ने अपनी भूमि वापस ली।
- कामगार खान ने रामगढ़ को नष्ट कर दिया।
शांति संधि और क्षेत्रों का विभाजन
- समझौते के तहत:
- रामपुर और जगोदीह लौटाए गए।
- कामगार खान को बराकर नदी के उत्तर का क्षेत्र मिला।
- विष्णु सिंह को नदी के दक्षिण का क्षेत्र मिला।
अंतिम विद्रोह और ब्रिटिश प्रतिक्रिया
- विष्णु सिंह ने फिर नवाब के विरोधियों से साजिश की।
- 1763 में नवाब मीर क़ासिम ने मार्कट खान के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा।
- विष्णु सिंह पराजित हुआ।
- सभी ज़मींदारों को भूमि वापस मिली।
- मार्कट खान ने छै परगना का उत्तरी भाग नवाब के लिए रख लिया।
मुकुंद सिंह का अवसरवाद और पराजय
- विष्णु सिंह की मृत्यु के बाद मुकुंद सिंह रामगढ़ का राजा बना।
- उसने बीघा और इतखोरी किलों पर कब्जा कर लिया और हथियार हासिल किए।
- 1766 में वारिस खान की अगुवाई में उसे हराया गया।
- मुकुंद सिंह ने सहमति दी:
- ₹27,000 बकाया कर चुकाने की
- बदले में छै पर अधिकार पाने की
अंतिम समझौता और प्रशासनिक विभाजन
- अगले वर्ष मुकुंद सिंह ने छै को पुनः रामगढ़ में मिला दिया।
- छै परगना को पाँच भागों में विभाजित किया गया:
- रामपुर
- जगोदीह
- परवारिया
- इतखोरी
- पीटी
उपनिवेशी विजय की भूमिका
- सिंहभूम, छोटानागपुर, पलामू और रामगढ़ की बिखरी स्थिति ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी।
- 1707–1765 का काल झारखंड में:
- रियासतों की खंडित स्थिति
- विश्वासघात
- सैन्य संघर्षों से भरा था
- मुग़ल शक्ति की कमी ने स्थानीय शासकों को जन्म दिया जिन्हें:
- मराठों या
- बंगाल के नवाबों ने नियंत्रित किया
- ब्रिटिश धीरे-धीरे किनारे से सत्ता में प्रवेश कर गए—कुछ ने स्वागत किया, कुछ ने विरोध।
अभियान और युद्ध
- जनवरी 1767: फरगुसन को सिंहभूम आक्रमण की जिम्मेदारी मिली।
- फरगुसन ने:
- झाड़ग्राम के राजा को पराजित किया।
- रामगढ़, जामबनी और सिलदा के राजाओं से आत्मसमर्पण करवाया।
- जामवनी में धालभूम के राजा को हराया।
- 22 मार्च 1767: धालभूम के जलते राजमहल पर कब्जा।
- जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया, बाद में नीमू ढाल को प्रतिस्थापित किया गया।
सिंहभूम में संधियाँ
- 1773: पोरहाट के राजा से एकरारनामा – कम्पनी के व्यापारियों और रैयतों को शरण न देने का वादा।
- बाद में सरायकेला और खरसावां ने भी ऐसी ही संधियाँ कीं।
कोल्हान और ‘हो’ जनजाति
- ‘हो’ क्षेत्र कोल्हान पर न मुगल और न ही मराठा शासन कर सके।
- स्वतंत्रता प्रेमी ‘हो’ जनजाति ने नागवंशी क्षेत्रों पर आक्रमण किए (1770, 1800)।
- मार्गों की असुरक्षा से व्यापार बाधित हुआ; कम्पनी ने हस्तक्षेप करना शुरू किया।
अंग्रेजों के सैन्य अभियान
- 1820: मेजर रफसेज का हमला, आंशिक सफलता।
- 1821: कर्नल रिर्चड के नेतृत्व में बड़ा हमला, ‘हो’ जनजाति ने आत्मसमर्पण किया।
- शर्तें:
- हल के हिसाब से कर देना (पहले 50 पैसा, फिर 1 रुपया प्रति हल)।
- व्यापारियों और यात्रियों की सुरक्षा।
- 1831–32: कोल विद्रोह में ‘हो’ सक्रिय रहे।
- 1836–37: फिर से विद्रोह और फिर आत्मसमर्पण।
- ‘हो’ क्षेत्र में ब्रिटिश प्रशासनिक इकाई स्थापित की गई।
पलामू और छोटानागपुर में कम्पनी का विस्तार
पलामू पर कब्जा (1771)
- पलामू की स्थिति:
- चेरो राजाओं (चिरंजीत राय और जयनाथ सिंह) का कब्जा था।
- अंग्रेजों ने गोपाल राय का समर्थन किया।
- जनवरी 1771: कैप्टन जैकब कैमेक को पलामू अभियान का आदेश मिला।
- 21 मार्च 1771: पलामू किला पर कब्जा।
- जुलाई 1771: गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया गया।
- मालगुजारी तय: 12,000 रुपये वार्षिक।
- चेरो राजा रामगढ़ भाग गए।
छोटानागपुर नागवंशी राजा की अधीनता
- दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की।
- सालाना 12,000 रुपये कर देने और मराठों के विरुद्ध सहायता का वचन दिया।
- कैमेक और दर्पनाथ शाह के बीच पगड़ी और टोपी बदलकर समझौते की पुष्टि हुई।
रामगढ़ और हजारीबाग
- रामगढ़ के राजा मुकुन्द सिंह अंग्रेजों का प्रारंभ में विरोध करते रहे।
- पड़ोसियों और अंग्रेजों के दबाव के कारण उसने बाद में मित्रता का प्रस्ताव भेजा।
- रामगढ़, हजारीबाग, और अन्य क्षेत्रों में धीरे-धीरे कम्पनी का प्रभाव बढ़ता गया।
- दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों का झारखंड पर कब्जा एक क्रमिक और रणनीतिक प्रक्रिया थी।
- आपसी संघर्ष, अराजकता और स्थानीय राजाओं की कमजोरियों का अंग्रेजों ने भरपूर फायदा उठाया।
- 1837 तक झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों पर कम्पनी का मजबूत नियंत्रण स्थापित हो चुका था।
लोहरदगा एजेन्सी का गठन और प्रशासन
- मुख्यालय: लोहरदगा के किसनपुर में स्थापित किया गया।
- प्रथम एजेन्ट: थॉमस विल्किन्सन, जो सीधे गवर्नर जनरल के प्रति जवाबदेह थे।
- लोहरदगा एजेन्सी का प्रधान जिला था।
- जिला अधिकारी: रॉबर्ट आउस्ले नियुक्त हुए।
1854 के बाद:
- साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी समाप्त कर दी गई।
- सम्पूर्ण छोटानागपुर को बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन किया गया।
- नॉन-रेगुलेशन प्रांत के रूप में नया प्रशासनिक ढाँचा बना।
- चुटियानागपुर कमिश्नरी का गठन:
- इसमें लोहरदगा, हजारीबाग, मानभूम, सिंहभूम, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, गंगापुर आदि राज्य शामिल थे।
मानभूम क्षेत्र
- ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में मानभूम का क्षेत्र बड़ा था, जिसमें झरिया, कतरास, पर्रा, रघुनाथपुर, करीह, झालदा, जयपुर, हेसला, बालमुंडी, ईचागढ़, बलरामपुर, पंचेत, अभियनगर, चतना और बड़ाभूम शामिल थे।
- 1767 में फरगुसन के मानभूम प्रवेश के समय पाँच बड़े स्वतंत्र जमींदार थे:
- मानभूम, बड़ाभूम, सुपुर, अभियनगर और चतना।
अंग्रेजों का संघर्ष:
- स्थानीय प्रजा अनुशासनहीन और विद्रोही हो गई थी।
- सैनिक कार्रवाई से सफलता नहीं मिलने पर सालाना बन्दोबस्त की नीति अपनाई गई।
- मानभूम के बाद सिंहभूम, सरायकेला और खरसांवा पर नियंत्रण का प्रयास किया गया, जो दशकों तक पूर्ण नहीं हो सका।
सिंहभूम और कोल्हान
- 1837 में कैप्टन विल्किन्सन ने कोल्हान पर हमला किया।
- इपिलासिंगी और पंगा गाँव जला दिए गए।
- आत्मसमर्पण के बाद कोल्हान गवर्नमेंट इस्टेट का गठन हुआ।
- पहला उपायुक्त: टिकेल नियुक्त हुए।
- विल्किन्सन रूल्स (1833): 31 नियमों का प्रशासनिक कोड लागू किया गया।
सरायकेला और खरसांवा:
- सरायकेला: क्षेत्रफल लगभग 700 वर्ग किमी।
- खरसांवा: क्षेत्रफल लगभग 225 वर्ग किमी।
- 1934 में दोनों क्षेत्रों को ब्रिटिश राज्य में शामिल किया गया।
संथाल परगना
प्रारंभिक ब्रिटिश नीति:
- पहाड़ी जनजातियाँ (‘हाईलैंडर’, ‘हिल मैन’) से शांति स्थापना का प्रयास।
- आदिम जनजातियाँ आखेट और लूट पर आश्रित थीं।
- मनीहारी के खेतौरी परिवार के अधीन इनका प्रशासन था।
- मानसिंह ने लकड़ागढ़ किला जीतने में सहायता की थी और इन पहाड़ियों का नियंत्रण प्राप्त किया था।
उपद्रव और ब्रिटिश प्रतिक्रिया:
- 18वीं सदी में मालेरों ने लकड़ागढ़ पर हमला किया।
- 1770 के अकाल के दौरान लूटमार में वृद्धि हुई।
- राजमहल और गंगा के दक्षिणी तट पर भय का माहौल।
- सरकारी हरकारों पर भी हमले हुए।
सैन्य कार्रवाई और प्रशासनिक सुधार
कैप्टन ब्रुक (1771-1774):
- 800 सैनिकों के साथ “मिलिटरी गवर्नर” नियुक्त।
- 283 गाँव बसाए।
- जंगलों में फैले आतंक का दमन किया।
कैप्टन जेम्स ब्राउन (1774-1778):
- परंपरागत जनजातीय संरचना को मान्यता देने का प्रस्ताव।
- सरदार-नायब-माँझी प्रणाली के अनुसार शासन व्यवस्था।
- चौकीबंदी का सुझाव और स्थानीय पुलिस प्रणाली की नींव।
अगस्तुस क्लीवलैंड और शांति स्थापना (1779-1784)
- पहाड़ियाओं के साथ न्याय और मानवीय नीति अपनाई।
- पहाड़ी सरदारों से मित्रता स्थापित।
- क्लीवलैंड योजना:
- पहाड़ियों को कृषि और सैनिक सेवा में जोड़ना।
- 400 माँझियों की सेना तैयार करना।
- सैनिकों को वेतन और वस्त्र प्रदान करना।
- क्लीवलैंड को राजमहल पहाड़ियों में सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है।
झारखंड में क्लीवलैंड और पहाड़िया व्यवस्था का प्रभाव
- क्लीवलैंड की पहाड़िया नीति:
- क्लीवलैंड ने पहाड़िया लोगों के जीवन में सुधार के लिए कई योजनाएँ बनाई।
- उसने बाजारों की व्यवस्था की और पहाड़िया लोगों को शिकार, मोम, खाल, शहद जैसे उत्पाद बेचने के लिए प्रोत्साहित किया।
- पहाड़िया लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उन पर कर नहीं लगेगा और उनके मुखिया ही उनके प्रशासनिक अधिकारी होंगे।
- क्लीवलैंड की नीति का प्रभाव:
- क्लीवलैंड की नीति ने पहाड़िया लोगों के बीच शांति और स्थिरता लाई।
- मि. वार्ड की टिप्पणी के अनुसार, क्लीवलैंड के बाद भी शांति बनी रही और अपराध बहुत कम हुए।
- क्लीवलैंड की योजनाओं का टूटना:
- क्लीवलैंड की योजनाएँ उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी नहीं रहीं।
- पहाड़िया पंचायतें अस्त-व्यस्त हो गईं और योजनाएँ बंद हो गईं, जैसे कि विद्यालयों का बंद होना और कुटीर उद्योग की योजनाएँ अधूरी रह गईं।
- क्लीवलैंड की ‘हिल रेंजर्स’ को भी उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई, जितनी अपेक्षित थी।
- हेस्टिंग्स का सुधार प्रयास:
- मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स ने क्लीवलैंड की योजनाओं में सुधार करने की कोशिश की, जैसे कि खेती के उपकरण और बीज भेजने का वादा, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया।
- फोम्बेल का सुधार:
- मि. फोम्बेल ने पहाड़िया व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद के शासकों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई।
- उसने 1796 के अधिनियम में बदलाव किया, जिससे पहाड़िया पंचायतों को मजिस्ट्रेट के अधीन लाया गया।
- अब्दुल रसूल खान का भ्रष्टाचार:
- बाद में, अब्दुल रसूल खान ने क्षेत्र का नियंत्रण लिया, लेकिन उसकी अत्याचारपूर्ण शासन के कारण जनमानस में असंतोष बढ़ा।
- संतालों का आगमन और शोषण:
- संतालों ने भागलपुर और वीरभूम में बसने की शुरुआत की और बाद में दामिन-ई-कोह में बड़ी संख्या में बस गए।
- उनका शोषण करने के लिए महाजनों ने कर्ज़ प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे संताल कर्ज में फंस गए और उन्हें न्याय की कमी का सामना करना पड़ा।
- संताल विद्रोह:
- 1855 में संतालों का विद्रोह, जिसे ‘हुल’ कहा जाता है, उत्पन्न हुआ। यह शोषण, भ्रष्टाचार और सरकारी उपेक्षा का परिणाम था।
- विद्रोह का कारण सरकारी अधिकारियों की अनुपस्थिति, महाजनों द्वारा अत्यधिक सूद वसूली और पुलिस की भ्रष्टाचारपूर्ण भूमिका थी।
- प्रशासनिक स्थिति:
- दामिन-ई-कोह में न्याय और प्रशासन की स्थिति बिगड़ गई थी, जहां संतालों को न्याय पाने के लिए भागलपुर और देवघर जाना पड़ता था।
- संतालों के पास सीमित संसाधन और अत्यधिक शोषण के कारण उनका जीवन कठिन हो गया।
- संतालों का संघर्ष:
- संताल अपनी आदतों, कर्ज़ और प्रशासनिक असुविधाओं के कारण लगातार शोषण के शिकार हो रहे थे।
- उन्हें महाजनों और अधिकारियों से न्याय नहीं मिल रहा था, और यही कारण था कि संताल विद्रोह की ओर बढ़े।
संताल विद्रोह और उसके परिणाम: एक ऐतिहासिक विश्लेषण
संताल विद्रोह (1855-1856), जिसे “हुल” भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जनविद्रोह था। इस विद्रोह ने ना केवल संतालों के संघर्ष को उजागर किया, बल्कि ब्रिटिश सरकार को भारत के आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों की आवश्यकता का एहसास भी दिलाया। इस विषय पर आधारित एक ब्लॉग में निम्नलिखित बुलेट पॉइंट्स में जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है:
1. संतालों का शोषण और उनके विद्रोह के कारण
- संतालों को बँधुआ मजदूरी, अत्यधिक सूद दरों पर कर्ज, और भूमि का छीनना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
- जमींदार, महाजन, और ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण ने संतालों को विद्रोह के लिए मजबूर किया।
- संतालों की भूमि, जो वे जंगलों को साफ करके कृषि के लिए इस्तेमाल करते थे, को जमींदारों द्वारा छीन लिया जा रहा था।
2. सिद्धु-कान्हू और उनके संदेश का प्रभाव
- सिद्धु, कान्हू, चाँद और भैरव नामक चार भाइयों ने एक दैवी संदेश का प्रचार किया, जिसमें देवता ने संतालों को न्याय की ओर प्रेरित किया।
- 30 जून, 1855 को लगभग 10,000 संताल भोगनाडीह में इकट्ठा हुए, जहाँ उन्हें देवता का आदेश सुनाया गया और संतालों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया गया।
3. विद्रोह की शुरुआत और संघर्ष
- संतालों ने 7 जुलाई 1855 को दारोगा महेशलाल दत्त की हत्या कर दी, जब वह उन्हें सरकारी आदेशों का पालन करने के लिए कहने पहुंचे थे।
- इसके बाद संतालों ने भागलपुर और वीरभूम तक विद्रोह फैलाया और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया।
- संतालों की तीर-धनुष और कुल्हाड़ियों के साथ संघर्ष में ब्रिटिश सेना को कई बार पराजित किया।
4. ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया
- ब्रिटिश सरकार ने संताल विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक भेजे, जिनमें मेजर बरो और कर्नल बर्ड शामिल थे।
- अगस्त 1855 तक विद्रोह को नियंत्रण में लाने के प्रयास किए गए, लेकिन संतालों ने जंगलों में छिपकर संघर्ष जारी रखा।
- अंततः, 1856 तक, संतालों को ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित कर दिया गया, लेकिन संतालों का संघर्ष उनके अधिकारों के लिए जारी रहा।
5. संतालपरगना जिले का गठन और सुधार
- 1855 का रेगुलेशन XXXVII लागू किया गया, जिसके तहत दामिन-ई-कोह को भागलपुर और वीरभूम से अलग कर एक नया जिला संतालपरगना बनाया गया।
- इस नए जिले में चार अनुमंडल (दुमका, गोड्डा, देवघर, और राजमहल) बने और संतालों के लिए प्रशासनिक सुधार किए गए।
- गाँवों में मुखिया प्रथा को मान्यता दी गई, जिससे संतालों और प्रशासन के बीच सीधे संपर्क का रास्ता खुला।
6. ब्रिटिश प्रशासन की प्रतिक्रिया और सुधार
- संताल विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव किए और संतालों के अधिकारों के लिए सुधारों की दिशा में कदम उठाए।
- जमींदारों और महाजनों द्वारा संतालों का शोषण रोकने के लिए कानून बनाए गए और संतालों को अपनी भूमि का अधिकार वापस दिलाने का प्रयास किया गया।
7. विद्रोह के बाद के प्रभाव
- संताल विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह सोचने पर मजबूर किया कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकता है।
- इस विद्रोह ने भारतीय समाज में जागरूकता का संचार किया और भविष्य में हुए आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त किया।